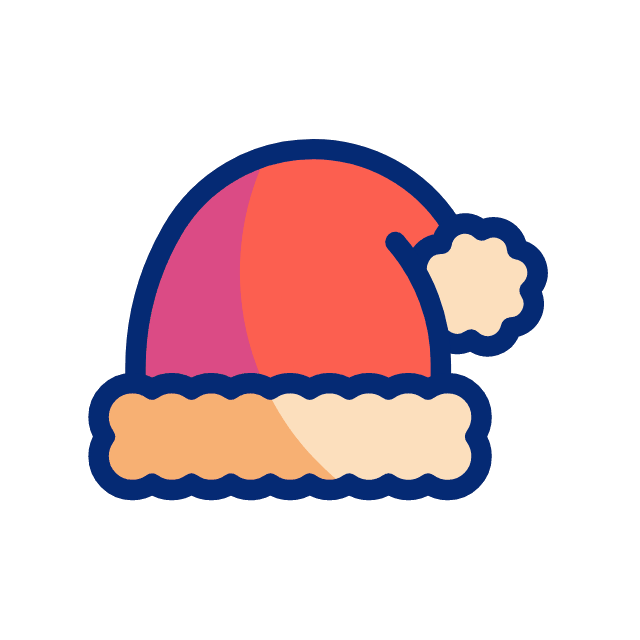बच्चों की परवरिश को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपनी संतान की देखभाल में कहीं से भी कोई कमी न रह जाए। इसके लिए वे अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर भी छोटी-छोटी बातों को लेकर कुछ पेरेंट्स ज्य़ादा ही परेशान हो जाते हैं। इसका उनके आपसी संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में बच्चे को अच्छी परवरिश देना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके संतुलित विकास के लिए उसकी सभी ज़रूरतों का खयाल रखना हर माता-पिता की पहली प्राथमिकता है लेकिन इसके लिए हमेशा चिंतित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं पर बिना कोई अतिरिक्त दबाव महसूस किए भी पेरेंटिंग से जुड़ी सभी जि़म्मेदारियों को सहज और सही ढंग से निभाया जा सकता है।
इस पेज पर:-

अच्छी नहीं है जल्दबाज़ी
घर में नए शिशु के आते ही माता-पिता उसे अच्छे ढंग से पालने की कवायद में जुट जाते हैं। वे उसके शारीरिक-मानसिक विकास को लेकर अनावश्यक ढंग से सजग रहते हैं। रोना-चिल्लाना, चीज़ें बिखेरना और जि़द करना जैसी बातें बच्चों की आदतों में सहज रूप से शामिल होती हैं। इसे लेकर चिंतित होना व्यर्थ है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास की गति को लेकर बेवजह तनावग्रस्त रहते हैं। वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हमउम्र बच्चों से अकसर उसकी तुलना करते हैं। दांत निकलने, चलना या बोलना सीखने के मामले में हर बच्चे के विकास की गति दूसरे से अलग हो सकती है।
अगर किसी दूसरे बच्चे की तुलना में आपका बेटा/बेटी दो-तीन महीने बाद चलना या बोलना शुरू करता/करती है तो इसके आधार पर अपने मन में यह नकारात्मक धारणा बना लेना अनुचित है कि मेरे बच्चे का शारीरिक-मानसिक विकास धीमी गति से हो रहा है। यह बात हमेशा याद रखें कि हर बच्चे की शारीरिक-मानसिक संरचना दूसरे से अलग होती है। इसलिए तुलना के आधार पर अपने बच्चे को कमतर समझना अनुचित है। हर बच्चा अपने आप में $खास होता है। इसलिए बेहतर यही है कि उसमें $खामियां ढूंढने के बजाय आप उसकी खूबियों को पहचानने की कोशिश करें।
खेल-खेल में सीखना
बच्चे अपने आसपास मौज़ूद हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश में जुटे रहते हैं। चीज़ें उठाना और उन्हें तोडऩा-गिराना जैसी हरकतों को अनुशासनहीनता समझकर उन्हें रोकने की कोशिश न करें। दरअसल इसी बहाने वे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तीन साल की उम्र से पहले बच्चे को अनुशासित करने की कोशिश व्यर्थ है। हां, उसके तीसरे जन्मदिन के बाद आप उसे प्यार से समझाते हुए उसकी ऐसी आदतों को धीरे-धीरे नियंत्रित करना शुरू करें लेकिन यह संभव नहीं है कि पहली बार में ही वह आपकी हर बात मान ले। अगर किसी एक $गलती के लिए बच्चे को कई बार टोकना पड़े तो इसे अपनी पेरेंटिंग की नाकामी न मानें क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे हर अभिभावक को दो-चार होना पड़ता है। हो सकता है, इससे आपको थोड़ी झल्लाहट हो पर अपने गुस्से को नियंत्रित रखना भी पेरेंटिंग का ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप अपना मन शांत रखेंगे तो बच्चों की छोटी-छोटी शरारतें आपको ज़रा भी परेशान नहीं करेंगी।
ज़रूरत आपसी सहयोग की
भारतीय समाज में आज भी ऐसा माना जाता है कि बच्चे की देखभाल मां की जि़म्मेदारी है लेकिन महानगरों के एकल परिवारों में रहने वाले कामकाजी दंपतियों की स्थिति थोड़ी अलग होती है। चूंकि पत्नी घर संभालने के साथ ऑफिस भी जाती है। ऐसे में बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पति का सहयोग ज़रूरी हो जाता है। सुबह उसे स्कूल भेजने की तैयारी और होमवर्क कराने जैसी सभी जि़म्मेदारियों में माता-पिता दोनों की भागीदारी ज़रूरी है। घर और ऑफिस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पति-पत्नी के बीच कार्यों का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को बहुत ज्य़ादा थकान न हो।
तमाम व्यस्तताओं के बावज़ूद थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें क्योंकि बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए आपका भी स्वस्थ और प्रसन्न रहना ज़रूरी है। रोज़मर्रा की छोटी-छोटी परेशानियों से पैदा होने वाले तनाव को $खुद पर हावी न होने दें। अगर किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो तो भी बच्चे के सामने ऊंची आवाज़ में बातचीत न करें क्योंकि वे चेहरे के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। माता-पिता के आपसी झगड़ों का बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अत: उनके सही भावनात्मक विकास के लिए हमेशा आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहे।
मज़बूत हो सपोर्ट सिस्टम
छोटे बच्चों की देखभाल अपने आप में फुल टाइम जॉब है, जिसमें थकान होना स्वाभाविक है। अगर आप कामकाजी हैं तो आपकी यह जि़म्मेदारी दोगुनी हो जाती है। इसलिए घर में एक मज़बूत सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की अच्छी देखभाल में प्रशिक्षित और कुशल घरेलू सहायिका आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। बेहतर यही होगा कि बच्चों के दादा-दादी या नाना-नानी भी उनके साथ ही रहें। इससे आपकी अनुपस्थिति में उन्हें प्यार भरा संरक्षण मिलेगा। अपने पड़ोसियों से भी आपके संबंध इतने सहज होने चाहिए कि ज़रूरत पडऩे पर आप उनसे बेझिझक मदद मांग सकें लेकिन इसे अपनी आदत न बनाएं, दूसरों की सुविधा का $खयाल रखना भी ज़रूरी है।
समझें बच्चे का नज़रिया
बच्चे के किसी भी व्यवहार को गलत मानकर उसे डांटने-फटकारने के बजाय एक बार उसकी परेशानियों को भी समझने की कोशिश करें। आजकल ढाई साल की उम्र से ही बच्चे प्ले स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। घर से बाहर निकल कर पहली बार किसी नए माहौल में जाकर वहां एडजस्टमेंट की कोशिश उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए अगर कभी आपका बच्चा रो-चिल्लाकर अपना गुस्सा ज़ाहिर करता है तो उसे धैर्यपूर्वक समझाने की कोशिश करें। अपने प्यार भरे व्यवहार से उसे सुरक्षा का एहसास दिलाएं।
इसे भी पढ़ें: क्या लटकने से बढ़ती है बच्चों की लंबाई, जानें सेहत से जुड़े ऐसे 10 सवालों के जवाब
थोड़ा सामाजिक बनें
अकसर लोगों की यह शिकायत होती है कि बच्चों की वजह से हमारी सोशल लाइफ $खत्म हो गई है क्योंकि उसे साथ लेकर आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। ऐसा न करें। माना कि उसे हर जगह अपने साथ ले जाना संभव नहीं है लेकिन आप अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फिर मेल-जोल बढ़ाएं, जिनके बच्चे आपके बेटे/बेटी के हमउम्र हों। उनके साथ अपने अनुभव शेयर करें। इससे बातों ही बातों में आपको पेरेंटिंग से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पेरेंटिंग को अलग कार्य समझने के बजाय यदि इसे जि़ंदगी का हिस्सा मान लिया जाए तो आप हमेशा तनावमुक्त रहेंगे।
ऐसे अन्य स्टोरीज के लिए डाउनलोड करें: ओनलीमायहेल्थ ऐप
Read More Articles On Parenting In Hindi
How we keep this article up to date:
We work with experts and keep a close eye on the latest in health and wellness. Whenever there is a new research or helpful information, we update our articles with accurate and useful advice.
Current Version