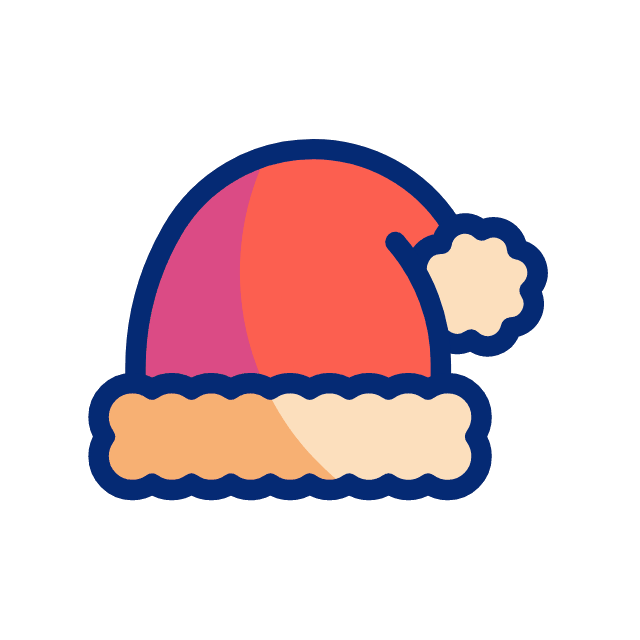Harmful Effects Of Hyper Parenting In Hindi: बच्चों की परवरिश कई तरह से की जाती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों को हर तरह के फैसले लेने की छूट देते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं, जो बच्चों को सही-गलत का फर्क समझाते हैं और उनकी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद बच्चों को ही लेने देते हैं। जबकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों से जुड़े सभी फैसले खुद करते हैं, जरूरत पड़े तो बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। पेरेंटिंग का यही स्टाइल हाइपर पेरेंटिंग कहलाता है। लेकिन ऐसी पेरेंटिंग से बच्चों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है।

हाइपर पेरेंटिंग के संकेत
- बच्चे की लाइफ से जुड़े हर निर्णय खुद लेना
- बच्चे को लेकर हर समय चिंतित रहना
- उसकी हर गतिविधी को कंट्रोल करना
- अपने बच्चे के उसकी मर्जी से दोस्त न चुनने देना
- बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना
इसे भी पढ़ें : आप कैसे कर रहे हैं अपने बच्चे की परवरिश? इन संकेतों से पहचानें कैसे पैरेंट हैं आप
हाइपर पेरेंटिंग के नुकसान
शारीरिक गतिविधियों में कमी: स्कूल ऑफ काइन्सियोलॉजी एंड हेल्थ स्टडीज, क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा के इयान जैनसेन ने 7 से 12 साल के बच्चों के 724 उत्तरी अमेरिकी माता-पिता पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन पेरेंट्स का आकलन किया गया, जो विभिन्न तरह के हाइपर पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हैं। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, टाइगर मॉम भी हाइपर पेरेंटिंग का ही एक रूप हैं। इस अध्ययन में माता-पिता की व्यस्तता और उनके बच्चों के बाहर खेलने, चलने या साइकिल चलाने और संगठित तरीके से खेल खेलने की आवृत्ति का आकलन किया गया। इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि हाइपर पेरेंट्स के बच्चे, विशेषकर जो 7 से 12 वर्ष के बीच हैं, उनमें फिजीकल एक्टिविटी कम देखी गई। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों और युवाओं को कम से कम 60 मिनट तक सामान्य रूप से फिजीकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। ऐसा करना, कार्डियोरेस्पिरेटरी और मांसपेशियों की फिटनेस, हड्डियों के स्वास्थ्य और हृदय और चयापचय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
इसे भी पढ़ें : बच्चों की परवरिश के ये 5 तरीके माने जाते हैं बहुत गलत, जानें कैसे पहुंचाते हैं बच्चों को नुकसान
हमेशा डरा-सहमा रहना: हाइपर पेरेंटिंग के दौरान पेरेंट्स अपने बच्चे को इस हद तक नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बच्चा खुद को किसी पिंजरे में कैद महसूस करता है। वह न तो खुलकर किसी से बात कर पात है और न ही दोस्त बना पाता। धीरे-धीरे वह अकेला रहने लगता है। अकेलेपन से जूझ रहे बच्चे को छोटे से छोटे काम करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे उसके मन में डर बैठ जाता है कि वह कुछ करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से वह अजनबियों से बातची करने में, लोगों से घुलने-मिलने में भी डर महसूस करता है।
हमेशा तनाव महसूस करना: जिन बच्चों की परवरिश में हाइपर पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाया जाता है, वे बच्चे अक्सर तनाव से ग्रस्त रहते हैं। दरअसल हाइपर पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। अगर बच्चे किसी कारणवश उन उम्मीदों को पूरा न कर सके, तो पेरेंट्स का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। यही बातें, बच्चे को अक्सर तनाव से ग्रस्त रखती हैं। इतना ही नहीं, पेरेंट्स की उम्मीदें पूरी न कर पाने की वजह से बच्चे अपराधबोध यानी गिल्ट से भी भर जाते हैं।
खुद पर भरोसा न करना: इस तरह के बच्चे खुद पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। असल में, पेरेंट्स अपने बच्चे को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उनके साथ बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। जब बच्चे के साथ निरंतर ऐसा होता है, तो वह मान लेता है कि वह किसी काम में सही नहीं है। उससे हर काम गलत ही होगा। इस तरह बच्चे में आत्मविश्वास की कमी बढ़ जाती है।
image credit : freepik
यह विडियो भी देखें
How we keep this article up to date:
We work with experts and keep a close eye on the latest in health and wellness. Whenever there is a new research or helpful information, we update our articles with accurate and useful advice.
Current Version